- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
तहखानों में बंद अक्स
देश-विदेश में अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता, सरोकारों और नारी-अस्मिता के लिए समर्पित लेखन के लिए सुपरिचित वरिष्ठ कथाकार-विचारक चित्रा मुद्गल की नई कृति ‘तहखानों में बंद अक्स’ स्त्री-विमर्श के बने-बनाए फ्रेम से एकदम अलग एक पठनीय कृति है।
समाज-सेवा से मिले व्यापक अनुभवों ने उन्हें ‘झुग्गी-झोपड़ियों में प्रेम’ को देखने की आत्मीय दृष्टि प्रदान की है, तो वह दूसरी औरत को भी समाज में बेगैरत नहीं मानतीं। सामाजिक समता का राग अलापने वाले समाज से वह आंख में आंख डालकर जो प्रश्न करती हैं, उससे हमारा ढोंगी समाज बेनकाब हो जाता है।
उनकी दृष्टि में स्त्री आज अपने लिए एक सम्मानजनक जगह चाहती है, रियायत नहीं। उनकी नजर समाज के हर वर्ग पर रहती है और उन दबावों पर भी जो आज युवतियों पर पड़ रहे हैं। वह उन्हें भयमुक्त करते हुए सहज जीवन की राह दिखाती हैं।
इस पुस्तक को पढ़ने वाली युवतियां न तो सड़कछाप मजनुओं से डरेंगी और न दहेज जैसी बुराइयों का सामना करने से। वह एक बेहतर पत्नी और मां तो बनेगी ही, उनमें सही सोच का निरंतर विस्तार भी होगा।
चित्राजी की कहानियों की तरह ये लेख भी पाठकों से अपना एक सीधा रिश्ता बनाते हैं। ‘तहखानों में बंद अक्स’ एक संग्रहणीय पुस्तक है।
अनुक्रम
- आवाजों को पुहारती आवाजें
- मड़ैया में प्रेम
- गठबंधन खुलि खुलि जाए
- दूसरी औरत बनाम समाज की गैरत
- भीतर दरकी सच्चाइयों का आईना
- वे कोई रियायत नहीं चाहतीं
- देह, दहेज और कुँवारियां
- आकाश में गूंजती अप्सराओं की चीख
- बदलते मुहावरे
- कुड़ियों का है जमाना
- टूटे हुए इन्द्रधनुषों का स्वयंवर
- मौन लोरियों का रुदन
- छौनों की गुहार
- नायिकाओं की उपेक्षा क्यों
- आप हरिजन को दामाद बनाएंगे?
- सूख रहे हैं बरगद
- फिल्मी भूमिकाओं में बचपन
आवाजों को गुहराती आवाजें
बिना फ्रेम के कुछ दृश्य अंतरचेतना की अदृश्य पिटारी में कुछ इस तरह से स्थिर हो जाते हैं कि बीत गए और बीतते समय के काले अंधड़ भी उन्हें, अपनी कील से उखाड़ नहीं पाते।
विस्मय होता है कि वे धुंधला तक नहीं पाए। शायद कोई रहस्यमय भीति, उन्होंने स्वयं अपने इर्द-गिर्द चुन रखी है। ताकि सुरक्षित रह सके स्त्री का छलनी हुआ अस्तित्व। ताकि जब भी उसे देखना हो अपने भूगोल और इतिहास की लहू रिसती सांधों को अविचलित देख सके वह उन दृश्यों को गौर से। बन सके स्वयं ही स्वयं के लिए साक्षी। क्योंकि सच के झुलसा देने वाले ताप को सह पाना सामान्यजन के बूते का नहीं। उनके बूते का तो हरगिज नहीं जो उत्तरदायी हैं उसके ‘स्व’ को अनदेखा करने के लिए।
एक ऐसा ही दृश्य जहन में कभी-कभी आंखें खोलता है और विवश करता है अपनी ओर देखने के लिए।
गांव वाले घर की बाई खमसार के अंतिम छोर पर छत तक उठी, काली नक्काशीदार अलमारी के उस पार अवस्थित अपने अंधेरे कुप्प कमरे के भीतर, काठ के भारी-भरकम संदूक के ऊपर चढ़े संदूक पर रखे अपने सिंगार पिटारे से कंघी और आईना निकालकर अम्मा, ढिबरी की कांपती मटियाली उजास में अपने बाल संवारती हैं। मांग भरती हैं। आंखों में काजल आंजती हैं। माथे पर टिकुली टांकती हैं।
आखिरी बार आई में दाएं-बाएं कोणों से अपनी छवि निहारकर वे छवि समेत आइने को वापस सिंगार पिटारे में सहेज देती हैं।
पीठ पर झूल रहे अपने आंचल को सिर पर टिका, आंचल को नाक तक खींच लेती हैं।
फिर फूंक खाई ढिबरी को कमरे के भीतर के आले के हवाले कर माचिस मुट्ठी में चांप कमरे से बाहर आकर अम्मा किवाड़ों की सांकल चढ़ा देती हैं।
कायदा नहीं है उस घर का। उस घर का ही नहीं स्त्री की अंधेरी दुनिया के अधिकांश अंतरे-कोनों का। दिन के उजाले में घर की बहू मजाल कि सिर से पल्ला हटा आईने में अपना रूप निहार ले।
एक मुलाकात में मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारतीजी से कहा था। उन आईनों को मैं सिंगार पिटारे के अंधेरे तहखानों से मुक्त करना चाहती हूं। लेकिन हां, अपनी पारंपरिक छवि से स्त्री को उन आईनों से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वह औरत स्वयं।
Additional information
| Authors | |
|---|---|
| Binding | Hardbound |
| ISBN | |
| Language | Hindi |
| Pages | |
| Publishing Year | 2017 |
| Pulisher |


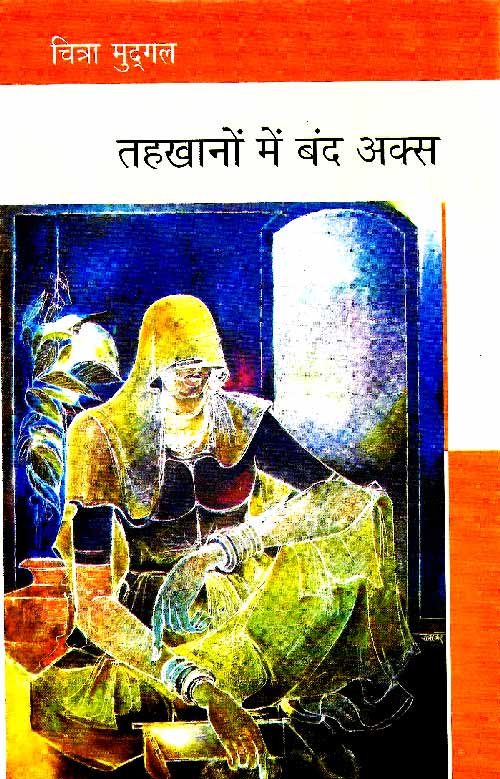





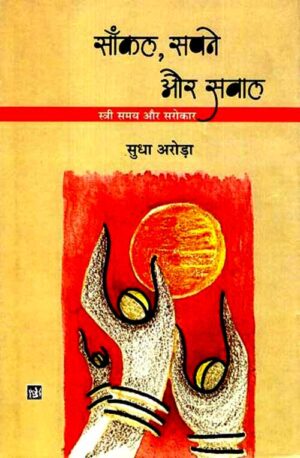
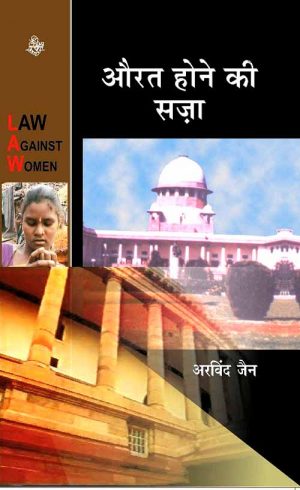
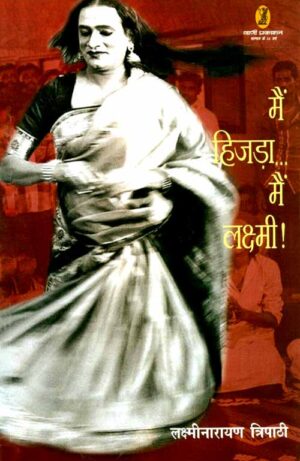




Reviews
There are no reviews yet.