- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
अब भी वसंत को तुम्हारी जरूरत है
रिल्के (1875-1926) जर्मन कवि ! रूस, पेरिस और इटली में यायावरी राहुल सांकृत्यायन भाव से ; घूमते-भटकते जिन्दगी काटी। शुरू की कविताएँ ‘हीनी’ और दूसरी लोक परम्पराओं की लय में लिखीं पर जल्दी ही अपनी अलग शैली विकसित कर ली, जहाँ संज्ञाएँ क्रियापदों का काम करती थीं और क्रियापद संज्ञा हो लेते थे, रोजमर्रा की जिन्दगी के साधारण प्रसंग और शब्द एक अलग तरह की ‘ईंजोत’ पा जाते थे, भाववाचक संज्ञाएँ ठोस वस्तुओं की ठाठ-बाट पा जाती थीं, अस्तित्व संधान से जुड़े यक्ष-प्रश्न भी अनौपचारिक-सा दोस्ताना तेवर अख्तियार कर लेते थे। एक आलोचक ने लिखा है कि उनकी कविता एक अजब तरह का तालमेल बिठाती है–‘‘अंदर की बेचैनी का—बाहरी चीजों की प्रशांति से।’’ अब जैसे ‘सेब का स्वाद’ जैसी छोटी-सी अनुभूति वहाँ छोटी-सी अनुभूति नहीं रहती, दार्शनिक आयामों वाला सुविचारित एक ठोस अनुभव-वृत्त बन जाती है। बच्चों औऱ जानवरों की ऐसी गहन, इन्द्रियगम्य उपस्थिति आधुनिक कविता में तो रिल्के ने ही पहले-पहल दर्ज की। रिल्के विश्व की प्रथम पंक्तियों के कवियों में अन्यतम हैं, क्योंकि उनके यहाँ रोजमर्रा की छोटी-से-छोटी अनुभूति भी एक बड़ा आयाम पा जाती है।
(रिल्के की कविताएँ)
अनुवाद की सीमाएँ
मुझे हमेशा से लगता रहा है—एक अच्छी कविता के विराट् अनुभव गह्वर से गुज़रना पुनर्जन्म के संतापविह्वल आह्लाद से गुज़रना है ! संवेदनशील ‘पाठ’ पाठक में कविता की पुनर्रचना का सुख जगाता है। हर पाठ में पाठक ही कविता को नए सिरे से रचते हों—ऐसा नहीं है, कविता भी पाठक को तोड़-तोड़कर नए सिरे से रचती-गढ़ती है ! पुनर्रचना की यह दोधारी प्रक्रिया तब और भी जटिल हो जाती है, जब पाठक का परिवेश, देश-काल, भाषा और भावबोध कविता के परिवेश, देश-काल, भाषा और भावबोध से भिन्न होता है, क्योंकि तब छेनी दोनों ओर से कई स्तरों पर चलती है, और सहसा समझ में नहीं आता—कहाँ क्या बना, क्या टूट गया !
उपनिवेश रह चुके देशों के औसत पाठक के लिए लंबे समय तक पश्चिमी भाषा और साहित्य नन्हीं एलिस का आश्चर्यलोक रहे हैं। हम ‘साहबों’ की भाषाएँ और साहित्य जानते हैं और नहीं भी जानते, समझते हैं और नहीं भी समझते, उसके मायाजाल से बाहर आना चाहते हैं और नहीं भी चाहते। उसका एक-एक शब्द, जिसमें हमें ठोकर लगती है, हाथ में उठाकर हम ऐसे जाँचते-परखते हैं, जैसे वह किसी नए पाताललोक के मुँह पर पड़ी चट्टान हो ! अनुवाद भी इसी जाँच-प्रक्रिया का हिस्सा माने जा सकते हैं। कैस्टेल सल्मन रुश्दी—जैसे प्रवासी भारतीयों को जिस लक्षणा से ‘अनूदित जीव’ कहते हैं (कैस्टेल 1990 : 25)—उसमें अपने मूल से कटकर एक नए निर्मम, असहानुभूतिशील परिदृश्य में अपनी अस्मिता स्थापित करने की पूरी पीड़ा समाहित है ! होमी भाभा (भाभा 1994:212) यह रूपक और आगे बढ़ाते हुए Translational Culture की बात करते हैं—सांस्कृतिक उत्पादों के आदान-प्रदान की एक नई भूमि है यह, जो विश्व को नई दृष्टि से आँकने की प्रक्रियाओं की साक्षी भी है। ठीक से देखें तो सांस्कृतिक अस्मिता के विघटन और पुननिर्माण की पूरी प्रक्रिया का संवहन ‘अनुवाद’ के हिस्से आ जाता है। और अनुवादों का प्राथमिक दायित्व यह बन जाता है कि वे रचना का सांस्कृतिक संदर्भ (corresponding cultural field for corresponding realities) प्रज्वलित करें। कुल मिलाकर स्थिति यह हो जाती है कि अनुवादक की समस्याओं का समाधान शब्दकोशों में उतना नहीं होता, जितना स्थानीय यथार्थों, पारंपरिक विधाओं और परिवर्तनगामी अस्मिताओं से भाषा का नाभिकीय बंध टटोलने में। इस प्रकार के उत्तर-औपनिवेशिक अनुवाद का एक भास्वर उदाहरण गायत्री स्पिवैक की किताब इमैजिनरी मैप्स है, जिसमें महाश्वेता देवी की तीन कहानियों की तिहरी (मार्क्सवादी, विसंरचनावादी, स्त्रीवादी) व्याख्या करती हुई वे उनके अनुवाद भी करती हैं ! इन अनुवादों की भाषा में एक ख़ास तरह का देशी ठस्सा है और अपने पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य (cultural ethos) को जस-का-तस अंग्रेज़ी में उठा लाने की कोशिश भी। ‘स्तनदायिनी’ नाम की कहानी का अनुवाद ‘द वेट नर्स’ न करके ‘द ब्रेस्ट गिवर’ वे करती हैं तो सिर्फ़ उसकी मार्क्सवादी/फ्रायडीय अनुगूँजों की ख़ातिर नहीं—बल्कि इसलिए कि ‘द वेट नर्स’ राष्ट्रीय अस्मिता से सर्वथा निरपेक्ष एक ठंडा, ब्रिटिश मुहावरा है। ‘मक्षिका स्थाने मक्षिका’ का अपना दर्शन भी कमोबेश यही करता है। मक्खी के स्थान पर मच्छर को बैठाया जा सकता है—पर तभी, जब किसी देश काल में मक्खी होती ही न हो और उसका सांस्कृतिक पर्याय वही मच्छर हो।
कमोबेश इन बातों का ध्यान में मैंने भी रखा है ! सजग रहने की कोशिश की है कि पाठ की अस्मिता बरक़रार रहे, यदि भाषाई तेवर में चस्पा न होने वाले मुहावरों में संदर्भगत फेर-बदल करने ही पड़ें तो वे ऐसे न हो जाएँ कि अर्थ का अनर्थ हो ले। पर कुल मिलाकर यह जटिल अनुभव था। एक बात जिसकी तरफ़ मेरा ध्यान ख़ास तौर पर गया, वह यह कि बड़ी कविता विषय-चयन से लेकर शब्द-चयन, बिम्ब, कथ्य, रूपक, कथन-भंगिमा आदि कई स्तरों पर हमें इतना चमत्कृत करती है कि कई बार अनुवाद करते हुए आदमी की अपनी रचनात्मक उठान लगती है ज़ोर मारने। रचनात्मकता के ज़ोर मारते ही आदमी पाठ के साथ शाहाना मनमानियाँ करने को प्रस्तुत हो जाता है जो न अनुवाद के हित में अच्छी बात होती है, न अनुवादक के हित में। इस तरह से देखा जाए तो अनुवाद आत्मानुशासन के पाठ भी पढ़ाता है। अपने प्रिय कवियों की रचना प्रक्रिया से सार्थक संवाद के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से छायाएँ पकड़ने का, परकायाप्रवेश का यह रोचक, पर जटिल खेल अपने-आप में एक बड़ा शैक्षिक अनुभव भी है, जो बहुत-सारे रचनात्मक अवगुंठन खोलता है और अनुवाद के रचनात्मक लेखन को प्रकारांतर से नए आयाम भी देता है।
पर जैसा मैंने पहले भी कहा—परकाया प्रवेश के इस रोचक, जटिल खेल के जितने सुख हैं, उतनी चुनौतियाँ भी। एक घर की बेटी के दूसरे घर की बहू बनकर प्रकृतस्थ होने में जितने बखेड़े नहीं होते, उससे कहीं अधिक महीन बखेड़े एक भाषा की कविता को दूसरी भाषा की कविता में प्रकृतस्थ कराने में होते हैं और इस क्रम में अनुवादक की भूमिका संयुक्त परिवार की सास-सी मारक और दुरूह होती है—इधर का तार उधर मिलाना चाहा, उधर का तार इधर और कुल मिलाकर इधर से गए और उधर से भी। पर अनुवाद के इस दोहरेपन में ही उसका सौंदर्य होता है—दो के योग से बनी एक तीसरी चीज़, जो न तो पहले से दूर जाकर जीवित रह सकती है, न दूसरे को छोड़कर। इसी दोहरेपन को साधने की कोशिश में इन अनुवादों का जन्म हुआ है। ये पाठक में यदि रिल्के की कविता के प्रति थोड़ी-सी भी उत्सुकता जगा सके तो अपना श्रम सार्थक समझूँगी।
उनकी लंबी और संदर्भ-गर्भित कविताओं का अनुवाद और अधिक दत्तचित्त श्रम की अपेक्षा रखता है। अँगरेज़ी साहित्य के अपने प्रिय छात्र और जर्मन भाषा के प्रखर अध्येता, सिद्धार्थ के वापस जर्मनी चले जाने से मेरा सीमित जर्मन-ज्ञान सिर्फ़ अँगरेज़ी का मुखापेक्षी होकर रह गया। अकेले लंबी कविताएँ उठाने का आत्मविश्वास हुआ नहीं !
अर्थलय बरक़रार रखने की कोशिश की है। रिल्के-जैसी नैसर्गिक सांगीतिकता सँभालनी तो मुश्किल थी, यति-भंग न हो—बस इसका ध्यान रखा। केन्द्रीय बिम्ब उभारने की कोशिश की। हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल वाक्य-रचना तोड़ी-मरोड़ी ! कुल मिलाकर इसका आभास तो मिला कि अनुवाद सचमुच ज़ंजीर-नृत्य है—हाथ-पाँव बँधे हुए हों, फिर भी कुछ घुमरियाँ ले ही लेता है आदमी !
शीर्षक बदल देने की धृष्टता की है। केन्द्रीय पंक्तियाँ सिर पर बिठा दी हैं, ताकि अलग से चमकें—नई भाषा में प्रवेश नए शहर में प्रवेश की मानिन्द होता है—सिर पर लदी गठरी में ही आपका समूचा वजूद बँधा रहता है—वही आपकी नई पहचान होती है—यह सोचकर ही शीर्षक की गठरी का ‘डेक्रॉन’ बदला है।
Additional information
| Authors | |
|---|---|
| Binding | Paperback |
| ISBN | |
| Language | Hindi |
| Pages | |
| Publishing Year | 2019 |
| Pulisher |





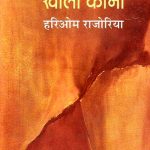


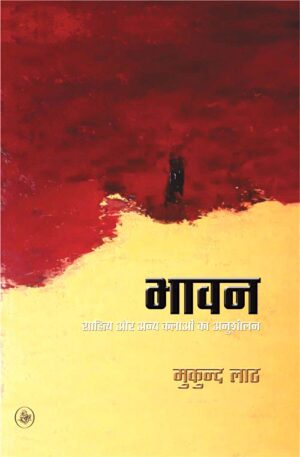





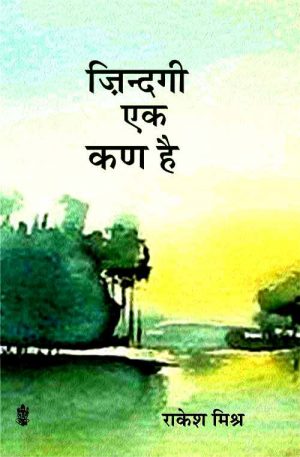
Reviews
There are no reviews yet.