- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Description
मानव मूल्य और साहित्य
‘‘सांस्कृतिक संकट या मानवीय तत्त्व के विघटन की जो बात बहुधा उठायी जाती रही है उसका तात्पर्य यही रहा है कि वर्तमान युग में ऐसी परिस्थियाँ उत्पन्न हो चुकी है जिनमें अपनी नियति के इतिहास निर्माण के सूत्र मनुष्य के हाथों से छूटे हुए लगते हैं। मनुष्य दिनों-दिन निरर्थकता की ओर अग्रसर होता प्रतीत होता है। यह संकट केवल आर्थिक और राजनीतिक संकट नहीं है वरन् जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से प्रतिफलित हो रहा है। यह संकट केवल पश्चिम या पूर्व का नहीं है वरन् समस्त संसार में विभिन्न धरातलों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है।’’
भूमिका
(प्रथम संस्करण से)
जब हम मानव मूल्य की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है। अपनी परिस्थितियाँ, इतिहास-क्रम और काल-प्रवाह के सन्दर्भ में मनुष्य की स्थिति क्या है और महत्त्व क्या है-वास्तविक समस्या इस बिन्दु से उठती है। समस्त मध्यकाल में इस निखिल सृष्टि और इतिहास-क्रम का नियन्ता किसी मानवोपरि अलौकिक सत्ता को माना जाता था। समस्त मूल्यों का स्रोत्र वही था और मनुष्य की एक मात्र सार्थकता यही थी कि वह अधिक से अधिक उस सत्ता से तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा करे। इतिहास या काल-प्रवाह उसी मानवोपरि सत्ता की सृष्टि था-माया रूप में या लीला रूप में।
ज्यों-ज्यों हम आधुनिक युग में प्रवेश करते गये त्यों-त्यों इस मानवोपरि सत्ता का अवमूल्यन होता गया। मनुष्य की गरिमा का नये स्तर पर उदय हुआ और माना जाने लगा कि मनुष्य अपने में स्वत: सार्थक और मूल्यवान् है-वह आन्तरिक शक्तियों से संपन्न, चेतन-स्तर पर अपनी नियति के निर्माण के लिए स्वत: निर्णय लेने वाला प्राणी है। सृष्टि के केन्द्र में मनुष्य है। यह भावना बीच-बीच में मध्यकाल के साधकों या सन्तों में भी कभी-कभी उदित हुई थी, किन्तु आधुनिक युग के पहले यह कभी सर्वमान्य नहीं हो पायी थी।
लेकिन जहाँ तक एक ओर सिद्धांतों के स्तर पर मनुष्य की सार्वभौमिक सर्वोपरि सत्ता स्थापित हुई, वहीं भौतिक स्तर पर ऐसी परिस्थितियाँ और व्यवस्थाएँ विकसित होती गयीं तथा उन्होंने ऐसी चिन्तन धाराओं को प्रेरित किया जो प्रकारान्तर से मनुष्य की सार्थकता और मूल्यवत्ता में अविश्वास करती गयीं। बहुधा ऐसी विचारधाराएँ नाम के लिए मानवतावाद के साथ विशिष्ट विशेषण जोड़कर उसका प्रश्रय लेती रही हैं। किन्तु: मूलत: वे मानव की गरिमा को कुण्ठित करने में सहायक हुई हैं और मानव का अवमूल्यन करती गयी हैं।
सांस्कृतिक संकट या मानवीय तत्त्व के विघटन की जो बात बहुधा उठाई जाती रही है, उसका तात्पर्य यही है कि वर्तमान युग में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं जिसमें अपनी नियति के, इतिहास-निर्माण के सूत्र मनुष्य के हाथों से छूटे हुए लगते हैं-मनुष्य दिनोंदिन निरर्थकता की ओर अग्रसर होता प्रतीत होता है। यह संकट केवल आर्थिक या राजनीतिक संकट नहीं है वरन् जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से प्रतिफलित हो रहा है। यह संकट केवल पश्चिम या पूर्व का नहीं है वरन् समस्त संसार में विभिन्न धरातलों पर विभिन्न रुपों में प्रकट हो रहा है।
प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य को इसी वर्तमान मानवीय संकट के सन्दर्भ में देखने की और जाँचने की चेष्टा की गयी है। साहित्य मनुष्य का ही कृतित्व है और मानवीय चेतना के बहुविध प्रयत्नरों (Responses) में से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रत्युत्तर है। इसलिए हम आधुनिक साहित्य के बहुत-से पक्षों को या आयामों को केवल तभी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जब हम उन्हें मानव-मूल्यों के इस व्यापक संकट के सन्दर्भ में देखने की चेष्टा करें।
अभी तक हिन्दी साहित्य के तमाम अध्ययनों में दो दृष्टिकोण लिये जाते रहे हैं। या तो हिन्दी साहित्य को अपने में एक संपूर्ण वृत्त मानकर उसका अध्ययन इस तरह किया जाता था जैसे वह शेष सभी बाहरी सन्दर्भों से विच्छिन्न हो। या इसका स्वरूप था कि उस पर बाहरी शक्तियों और धाराओं के प्रभावों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता रहा है गोया वह केवल निष्क्रिय तत्त्व है जिसे दूसरे केवल प्रभावित कर सकते हैं। किन्तु वह केवल दूसरे साहित्यों से ‘प्रभावित’ ही नहीं हुआ है वरन् विश्व इतिहास की समस्त प्रक्रिया में स्वयं एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उसने संकट का सामना किया है; नये मूल्यों के विकास की भूमिका प्रस्तुत की है और तमाम साहित्यों के बीच वह केवल दूसरों से प्रभावित होने की वस्तु ही नहीं रही है वरन् उन तमाम आधुनिक परिस्थितियों के बीच उसका अपना सहज स्वाभाविक उन्मेष हुआ है।
प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए पहले व्यापक सांस्कृतिक संकट का सर्वेक्षण किया गया है और तब उसके सन्दर्भ में हिन्दी साहित्य की बात की गई है। हिन्दी के प्रसंग में लेखक ने छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है क्योंकि उसके विचार में एक ने मूल समस्या का सामना ही नहीं किया और दूसरे ने समस्या को गलत परिप्रेक्ष्य में उठाकर उलझनें बढ़ा दीं। अपनी सहमति-असहमति को लेखक ने स्पष्ट और बलपूर्वक रखने की चेष्टा की है क्योंकि उसका विश्वास है कि चिन्तन के क्षेत्र में यह आवश्यक भी है और उपयोगी भी।
यह पुस्तक लगभग तीन वर्ष पूर्व ही पाठकों के सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियोंवश इसके प्रकाशन में विलम्ब होता गया। इसके लेखन के दौरान सर्वश्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, डॉ. रघुवंश, फादर आई.ए.एक्स्ट्रास, विजयदेव नारायण साही तथा डॉ.रामस्वरूप चतुर्वेदी से अक्सर विचार-विनिमय होता रहा है जिससे मेरे चिन्तन को बहुत प्रेरणा मिली है। मैं उन सबों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
Additional information
Additional information
| Binding | Paperback |
|---|---|
| Authors | |
| ISBN | |
| Language | Hindi |
| Pages | |
| Publishing Year | 2019 |
| Pulisher |


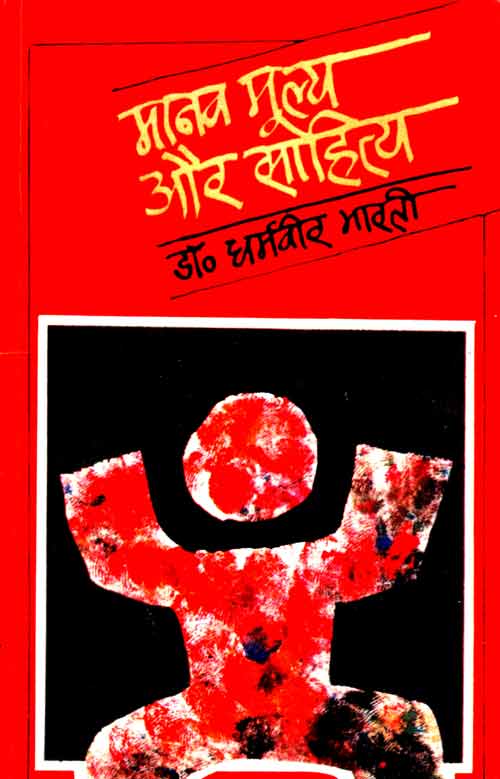




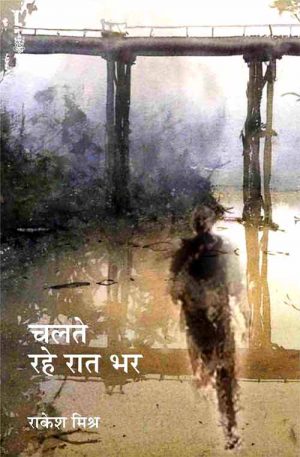
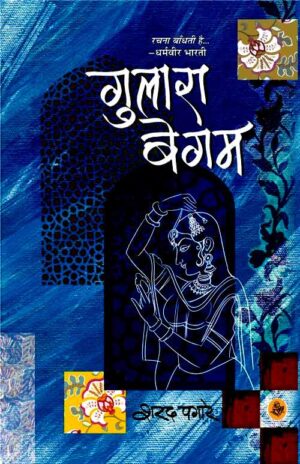


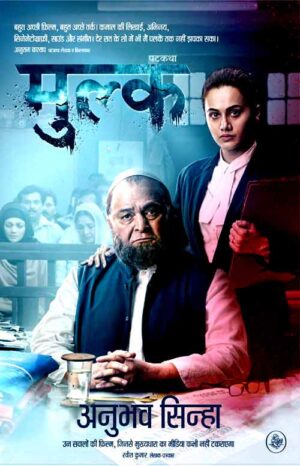
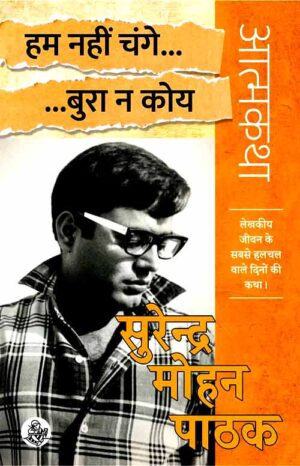
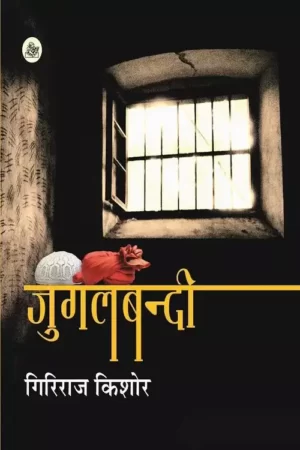

Reviews
There are no reviews yet.