- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
मृत्युंजय
1942 के स्वाधीनता आन्दोलन में असम की भूमिका पर लिखी गयी एक श्रेष्ठ एवं सशक्त साहित्यिक कृति है ‘मृत्युंजय’। असम क्षेत्रीय घटनाचक्र और इससे जुड़े हुए अन्य सभी सामाजिक परिवेश इस रचना को प्राणवत्ता देते हैं चरित्र समाज के उन स्तरों के है जो जीवन की वास्तविकता के बीभत्स रूप के दासता के बन्धनों में बँधे-बँधे देखते आये हैं और अब प्राणपन के संघर्ष करने तथा समाज की भीतरी-बाहरी उन सभी विकृत मान्यताओं को निःशेष कर देने के लिए कृतसंकल्प है।
उपन्यास में विद्रोही जनता का सजीव चित्रण है। विद्रोही की एक समूची योजना और निर्वाह, आन्दोलनकारियों के अन्तर-बाह्य संघर्ष, मानव- स्वभाव के विभिन्न रूप; और इन सबके बीच नारी-मन की कोमल भावनाओं को जो सहज, कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है वह मार्मिक है। कितनी सहजता से गोसाईं जैसे चिर-अहिंसावादी भी हिंसा एवं रक्तपात की अवांछित नीति को देशहित के लिए दुर्निवार मानकर उसे स्वीकारते हुए अपने आपको होम देते हैं ! और फिर परिणाम ? स्वान्त्र्योत्तर काल के अनवरत, उलझे हुए प्रश्न ?……
भारतीय ज्ञानपीठ को हर्ष है कि उसे असमिया की इस कृति पर लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने का गौरव मिला।
आमुख
(प्रथम संस्करण से)
लेखक के नितान्त अपने दृष्टिकोण से देखें तो पुस्तक के लिए किसी आमुख की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविकता इसी में रहती है कि पुस्तक और पाठक के बीच सम्प्रेषण निरवरोध हो। मेरे जैसे लेखक के लिए तो, जो अपनी रचना के प्रति अनासक्त रहना चाहता हो, आमुख लिखना और भी दुष्कर हो जाता है। पर प्रस्तुत पुस्तक के प्रसंग में कुछ लिखना शायद उपयोगी हो।
हमारे यहाँ साहित्यिक विद्या के रूप में उपन्यास पश्चिम से आया; और देखते-देखते इसने यहाँ घर कर लिया। भले ही हमारी परम्परा काव्य को मान्यता देती आयी, पर पाठक-जगत् ने उपन्यास को फिर भी युग का प्रतिनिधि सृजन रूप माना। रवि बाबू जैसे महान कवि प्रतिभाओं तक ने महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखे और इस विद्या को गरिमा प्रदान की। फिर तो उपन्यास न केवल समाज के लिए दर्पण बना, बल्कि सामायिक विचार-चिन्तन की अभिव्यक्ति का माध्यम भी हुआ।
मैंने स्वयं जब सामाजिक वास्तविकता की भाव-प्रेरणा पर उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया तब असमिया में यह विद्या काफी प्रगति कर चुकी थी। भविष्य इसका कैसा और क्या होगा, यह आशंका समाक्षकों के मन में अवश्य थी। हाँ विवेकी समीक्षक उस समय भी आश्वस्त थे। उनके विचार से असमी जीवन की विविधरूपता के कारण लेखक को सामग्री का अभाव कभी न होगा। और सचमुच देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सामाजिक वास्तविकता को आपसी तनावों ने ऐसा विखंडित कर रखा था कि लेखक के लिए सदाजीवी चुनौती बनी रहे।
जितना कुछ अब तक मैंने लिखा वह सब न अमृत ही है, न निरा विष। कुछ है तो ऐसे एक व्यक्ति का प्रतिबिम्ब मात्र, जो अमृत की उपलब्धि के लिए वास्तविकता के महासागर का मन्थन करने में लगा हो। मेरे प्रमुख उपन्यासों के प्रमुख पात्रों में ऐसा कोई नहीं जिसके अन्तर्मानस में एक सुन्दर और सुखद समाज की परिकल्पना हिलोरती न रहती हो। कहीं व्यक्तित्व रूप से तो कहीं सामूहिक रूप से, वे सभी इस महामारियों के मारे वर्तमान जीवन-जगत् की बीभत्स वास्तविकता को अस्वीकार ही अस्वीकार करते-रहते हैं। किन्तु सच्चाई यह भी है कि वे चरित्र-पात्र एक सम्भावनीय मानव-संसार के सम्भव प्राणी मात्र होतें हैं, और उस समूची परिकल्पना का सृजेता स्वयं भी सम्भवन की अवस्था में होता है।
उपन्यास-लेखन को सामने की वास्तविकता से ऊपर उठकर उसे विजित करना पड़ता है, तभी ऐसे चरित्रों की परिकल्पना और सर्जना सम्भव हो पाती है जो उसकी विचार-भावनाओं के प्रतीक और संवाहक बन सकें। सच तो, अपने अभीष्ट चरित्रों की खोज में उसे पल-घड़ी लगे रहना होता है। ऐसा न करे वह तो उसके भावित चरित्र उसी का पीछा किया करेंगे। और जहाँ अभीष्ट चरित्रों का रूपायन हुआ कि फिर उसे ऐसे कल्पना-प्रसूत लोक-परिवेश की रचना करनी होती है जहाँ वे सब रह सकें, सक्रिय हों, सोचें-विचारें और गन्तव्य की ओर बढ़ते जा सकें। अवश्य अपना एक-एक चरित्र उसे लेना होगा युगीन वास्तविकता से हीः और लेना भी होगा बिलकुल मूल रूप में : मृत चाहे जीवित। एक सीमा-बिन्दु तक पहुँचने के बाद फिर लेखक की ओर से रचित्र-पात्रों को छूट मिल जाती है कि अपने-अपने वस्तुरूप का अतिक्रम करें और उसकी अपनी भावनाओं और मूल्यों के साथ एकाकार हों।
वास्तव में सृजन प्रक्रिया को शब्द–बद्ध कर पाना कठिन होता है। किस प्रकार क्या-क्या करके रचना का सृजन हुआ, इसमें पाठक की रुचि नहीं होती। उसका प्रयोजन सामने आयी रचना पर तो सृजन-पीड़ा के कोई चिह्न कहीं होते नहीं। अनेक बार होता है कि अनेक चरित्रों के भाव-रूप अनेक-अनेक बरसों तक लेखन की चेतना के कोटरों में अधमुँदी आँखों सोये पड़े रहते हैं और फिर रचना-सृजन के समय उनमें से कोई भी हठात् आकर कथानक में भूमिका ग्रहण कर लेता है। ये तीनों उपन्यास- ‘इयारूइंगम’, ‘प्रतिपद और ‘मृत्युंजय’- लिखते समय ऐसा ही हुआ।
इनके चरित्र-पात्र समाज के उन स्तरों से लिये गये हैं जो सामाजिक वास्तविकता के बीभत्स रूप को देखते-भोगते आये हैं और अपनी स्वाभाविक मानवीयता तक से वंचित हो बैठे हैं। वे अब उत्कण्ठित हैं कि संघर्ष करें और यथार्थ मानव बन उठने के लिए अपने को भी बदलें और समूचे समाज को भी। किसी भी मूल्य पर वे अब सामाजिक बीभत्सता का अस्तित्व लुप्त कर देना चाहते हैं; और चाहते हैं कि समाज का बाहरी ही नहीं, भीतरी ढाँचा भी स्वास्थ और सहायक रूप ग्रहण करे।
‘मृत्युंजय’ की कथावस्तु है 1942 का विद्रोहः ‘भारत छोड़ों’ आन्दोलन का असम क्षेत्रीय घटना-चित्र और इसके विभिन्न अंगों के साथ जुड़ा–बँधा अन्य वह सब जो रचना को प्राणवत्ता देता है, समृद्धि सहज मानवीय भावनाओं के चिरद्वन्द्वों की अछूत छवियों द्वारा।
कथानक आधारित है वहाँ की सामान्यतम जनता के उस विद्रोह की लपटों को अपने से लिपटा लेने पर, और कैसा भी उद्गार मुँह से निकले बिना प्राण होम कर उसे सफल बनाने पर। घटना के 26 वर्ष बाद यह उपन्यास, मैंने लिखा। उस समय की वह आग ठण्डी पड़ चुकी थी; पर उसकी आत्मा, उसका यथार्थ, अब भी सांसें ले रहे थे। उपन्यास में विद्रोह-सिक्त जनता के मानस का, उसकी विभिन्न ऊहापोहों का चित्रण किया गया है। सबसे बड़ी समस्या उस भोले जनसमाज के आगे यह थी कि गाँधी जी के अहिंसावादी मार्ग से हटकर हिंसा की नीति को कैसे अपनाएं; और सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इतनी-इतनी हिंसा और रक्तपात के बाद का मानव क्या यथार्थ मानव होगा ? वह प्रश्न आज भी ज्यों-का-त्यों जहाँ का तहाँ खड़ा है।
भारतीय ज्ञानपीठ के प्रति मैं आभारी हूँ कि यह कृति हिन्दी पाठकों के सम्मुख पहुँच रही है। इसका हिन्दी रूपान्तर गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्ण प्रसाद सिंह ‘मागध’ ने किया है। मैं उनका आभारी हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक डॉ. रणधीर साहा का भी जिनका सक्रिय सहयोग इसे मिला।
Additional information
| Authors | |
|---|---|
| Binding | Hardbound |
| ISBN | |
| Language | Hindi |
| Pages | |
| Publishing Year | 2022 |
| Pulisher |




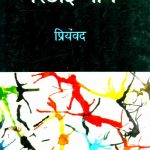


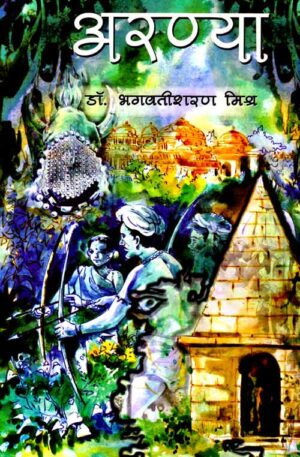
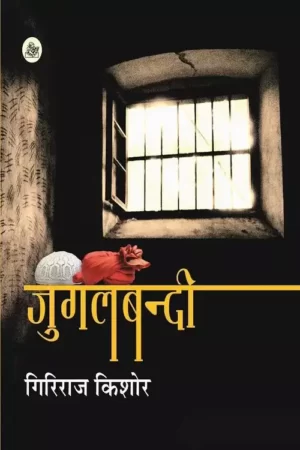
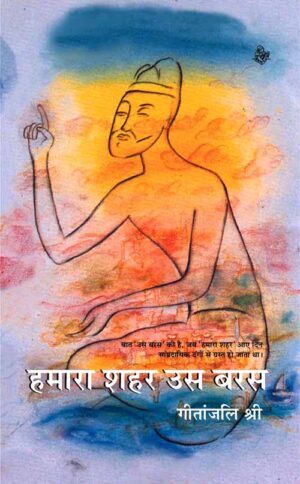




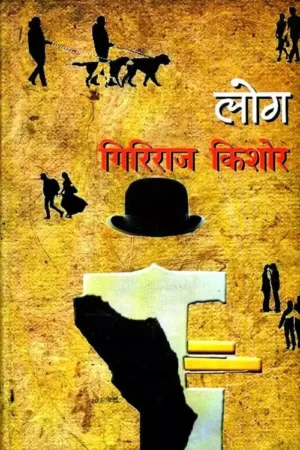
Reviews
There are no reviews yet.